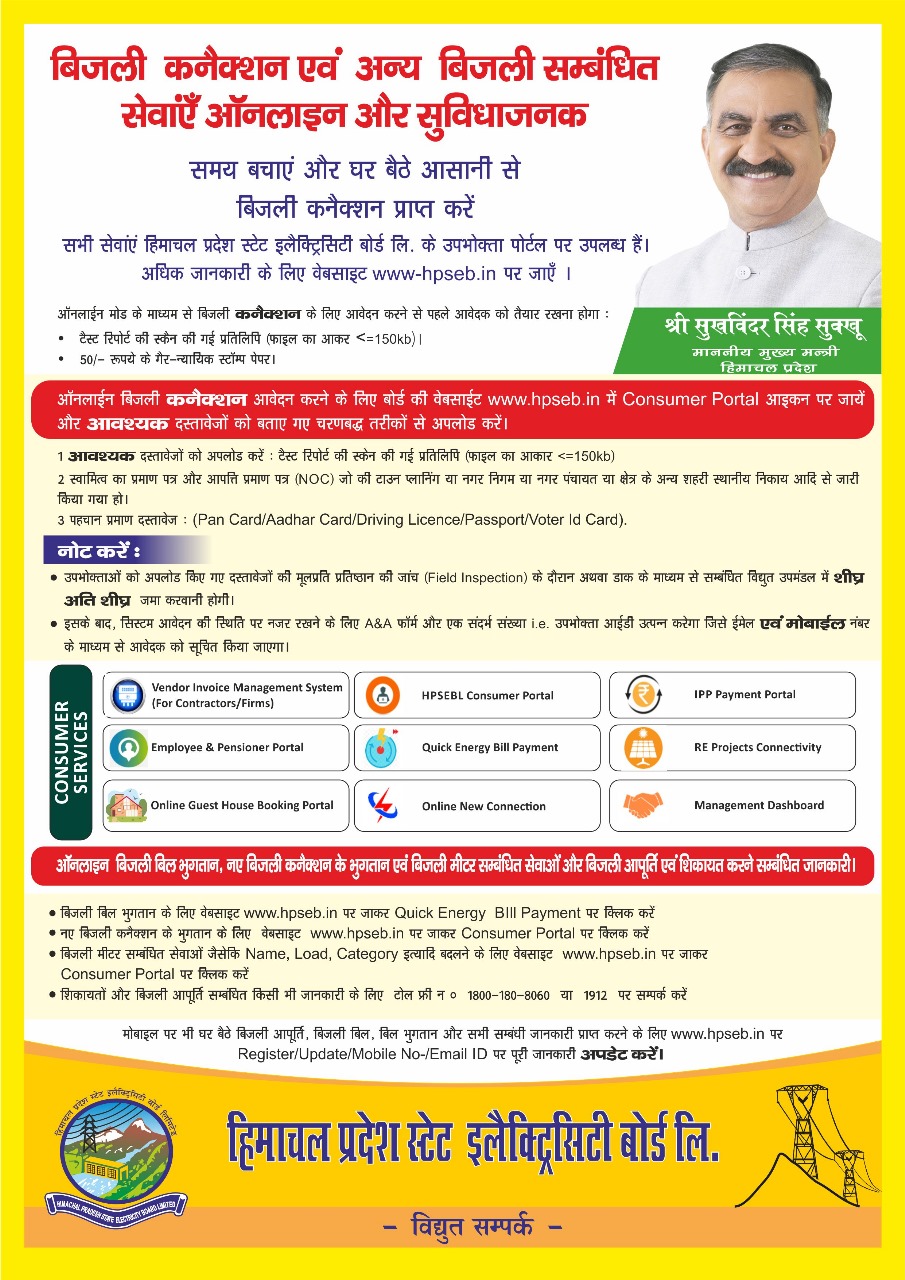ShareThis for Joomla!
घातक होंगे गांधी के चरित्र हनन के प्रयास
- Details
- Created on Tuesday, 01 March 2022 11:47
- Written by Baldev Sharma
 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चरित्र हनन और उनको मारने वाले नाथूराम गोडसे का महिमा मण्डन करते हुए सोशल मीडिया ओ.टी.टी. मंच लाईम लाईट पर आयी फिल्म ‘‘मैंने गांधी को क्यों मारा’’ के खिलाफ सर्वाेच्च न्यायालय में दायर हुई एक याचिका के माध्यम से इसके प्रसारण पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाये जाने का आग्रह किया गया है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में भी अधिवक्ता भूपेंद्र शर्मा ने इस आशय की एक याचिका दायर की है जिस पर अदालत ने सभी संबद्ध पक्षों को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। स्वभाविक है कि इस पर अब चर्चाओं का दौर चलेगा और एक वर्ग इस फिल्म के तथ्य और कथ्य को प्रमाणित सिद्ध करने का प्रयास करेगा। इस बहस के दूरगामी परिणाम होंगे। इसलिये इस संद्धर्भ में कुछ बुनियादी सवाल सामने रखना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जिन लोगों ने यह फिल्म बनायी है जो लोग इसका समर्थन या विरोध करेंगे और जो इस पर फैसला देंगे वह सभी लोग वह हैं जो 1947 के बाद पैदा हुये हैं। उनका आजादी की लड़ाई का अपना कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। सबकी जानकारियां अपने-अपने अध्ययन और उसकी समझ पर आधारित हैं। इस समय जो पार्टी केंद्र में सत्ता में है वह संघ परिवार की एक राजनीतिक इकाई है। संघ की स्थापना 1922 में हुई थी। उस समय संघ का राजनीतिक पक्ष हिंदू महासभा थी। संघ और हिंदू महासभा की स्थापना से लेकर 1947 में देश की आजादी तक इन संगठनों की आजादी की लड़ाई को लेकर रही भूमिका के संद्धर्भ में कोई बड़े नामों की चर्चा नहीं आती है। वीर सावरकर और बी एस मुंजे की जनवरी 1930 में हिटलर से हुई मुलाकात का जिक्र मुंजे की डायरी में मिलता है। जिसमें ऐसे युवा तैयार करने की बात कही गयी है जो बिना तर्क किये कुछ भी करने को तैयार हो जायें। दूसरी ओर कांग्रेस का गठन 1885 में हो जाता है और आजादी की लड़ाई में योगदान करने वालों की एक लंबी सूची उपलब्ध है। इसी सूची में महात्मा गांधी का नाम भी आता है। यह भी तथ्य है कि जब 1935 में अंतरिम सरकारें है बनी थी तब हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने बंगाल में संयुक्त सरकार बनाई थी। यह कुछ मोटे तथ्य हैं जिनका कभी कोई खण्डन नहीं आया है।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चरित्र हनन और उनको मारने वाले नाथूराम गोडसे का महिमा मण्डन करते हुए सोशल मीडिया ओ.टी.टी. मंच लाईम लाईट पर आयी फिल्म ‘‘मैंने गांधी को क्यों मारा’’ के खिलाफ सर्वाेच्च न्यायालय में दायर हुई एक याचिका के माध्यम से इसके प्रसारण पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाये जाने का आग्रह किया गया है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में भी अधिवक्ता भूपेंद्र शर्मा ने इस आशय की एक याचिका दायर की है जिस पर अदालत ने सभी संबद्ध पक्षों को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। स्वभाविक है कि इस पर अब चर्चाओं का दौर चलेगा और एक वर्ग इस फिल्म के तथ्य और कथ्य को प्रमाणित सिद्ध करने का प्रयास करेगा। इस बहस के दूरगामी परिणाम होंगे। इसलिये इस संद्धर्भ में कुछ बुनियादी सवाल सामने रखना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जिन लोगों ने यह फिल्म बनायी है जो लोग इसका समर्थन या विरोध करेंगे और जो इस पर फैसला देंगे वह सभी लोग वह हैं जो 1947 के बाद पैदा हुये हैं। उनका आजादी की लड़ाई का अपना कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। सबकी जानकारियां अपने-अपने अध्ययन और उसकी समझ पर आधारित हैं। इस समय जो पार्टी केंद्र में सत्ता में है वह संघ परिवार की एक राजनीतिक इकाई है। संघ की स्थापना 1922 में हुई थी। उस समय संघ का राजनीतिक पक्ष हिंदू महासभा थी। संघ और हिंदू महासभा की स्थापना से लेकर 1947 में देश की आजादी तक इन संगठनों की आजादी की लड़ाई को लेकर रही भूमिका के संद्धर्भ में कोई बड़े नामों की चर्चा नहीं आती है। वीर सावरकर और बी एस मुंजे की जनवरी 1930 में हिटलर से हुई मुलाकात का जिक्र मुंजे की डायरी में मिलता है। जिसमें ऐसे युवा तैयार करने की बात कही गयी है जो बिना तर्क किये कुछ भी करने को तैयार हो जायें। दूसरी ओर कांग्रेस का गठन 1885 में हो जाता है और आजादी की लड़ाई में योगदान करने वालों की एक लंबी सूची उपलब्ध है। इसी सूची में महात्मा गांधी का नाम भी आता है। यह भी तथ्य है कि जब 1935 में अंतरिम सरकारें है बनी थी तब हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने बंगाल में संयुक्त सरकार बनाई थी। यह कुछ मोटे तथ्य हैं जिनका कभी कोई खण्डन नहीं आया है।
इस परिदृश्य में जब 1947 में देश आजाद हुआ और साथ ही बंटवारा भी हो गया। तब जनवरी 1948 में गांधी जी की हत्या कर दी गयी। उसी दौरान 1948 और 1949 में संघ ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और हिंदुस्तान समाचार न्यूज़ एजेंसी की स्थापना कर ली। जब देश बंटवारे के जख्म और गांधी की हत्या के दंश सह रहा था तब संघ भविष्य के मीडिया और युवा शक्ति को अपने उद्देश्य के लिए तैयार करने की व्यवहारिक योजना पर काम करने लग गया था। आज दोनों ईकाईयां सत्ता में कितनी प्रभावी भूमिका निभा रही हैं यह किसी से छिपा नहीं है। यह कहा जाता है कि अंग्रेजों को भगाने के लिये गांधी बंटवारे पर सहमत हो गये थे। उनका विश्वास था कि वह दोनों टुकड़ों को फिर से एक कर लेंगे। गांधी के इस विश्वास की समीक्षा तब हो पाती यदि वह दो-चार वर्ष और जिंदा रहते। गांधी इतिहास के ऐसे मोड़ पर मार दिये गये जहां पर उनको लेकर उठाया जाने वाला हर सवाल बेईमानी हो जाता है। क्योंकि बंटवारे के छः माह के भीतर ही उनको रास्ते से हटा देना एक ऐसा कड़वा सच है जो उन पर उठने वाले सवालों का स्वयं ही जवाब बन जाता है।
संघ अपनी राजनीतिक इकाई जनसंघ के माध्यम सेे 1952 से चुनाव लड़ता आ रहा है। 2014 में भाजपा के नाम से पहली बार अपने तौर पर सत्ता पर काबिज हो पाया है। 1948 से लेकर आज तक संघ की कितनी ईकाईयां हैं और वह क्या-क्या कर रही हैं अधिकांश को पता ही नहीं है। संघ शायद पहली संस्था है जो पंजीकृत नहीं है और अपने स्नातक तक तैयार कर रही है। इसका पाठयक्रम क्या है किसी को कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं है। आज तक इसके कितने स्नातक निकल चुके हैं और किस किस फिल्ड में हैं इस पर आम आदमी का ध्यान गया ही नहीं है। इसका इतिहास लेखन प्रकोष्ठ और संस्कार भारती कब से स्थापित हैं और क्या कर रहे हैं शायद आम आदमी को जानकारी ही नहीं है। अभी धर्म संसदों के माध्यमों से यह सामने आया है कि मुस्लिम समुदाय को लेकर इनकी सोच क्या है। जबकि डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत तक दर्जनों ऐसे नेता हैं जिनके मुसलमानों के साथ एक और पारिवारिक रिश्ते हैं तो दूसरी ओर यह लोग सार्वजनिक मंचों से उनका विरोध करते हैं। आजादी की लड़ाई के दौरान किस तरह इनके नेता स्वतंत्रता सेनानियों की मुखबिरी करते थे इस संबंध में स्व.अटल जी के खिलाफ ही अदालती साक्ष्य लेकर स्वंय डॉ. स्वामी आये हैं। स्व.अटल जी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं लेकिन आजादी की लड़ाई के दौरान उनकी मुखबिरी वाली भूमिका से क्या उन्हें देश हित का विरोधी कहा जा सकता है। नहीं, उस समय उन्होंने ऐसा जो भी कुछ किया होगा अपने वरिष्ठों के आदेशों की अनुपालना में किया होगा। इसलिये आज गांधी नेहरू के चरित्र हनन और उन्हें पाठयक्रमों से हटाकर सच को दबाने के प्रयास देश हित में नहीं माना जा सकता। बल्कि यह माना जायेगा कि ऐसे प्रयासों से आर्थिक असफलताओं को दबाने का काम किया जा रहा है।
चुनाव आयोग की प्रसांगिता पर उठते सवाल
- Details
- Created on Monday, 21 February 2022 16:09
- Written by Shail Samachar





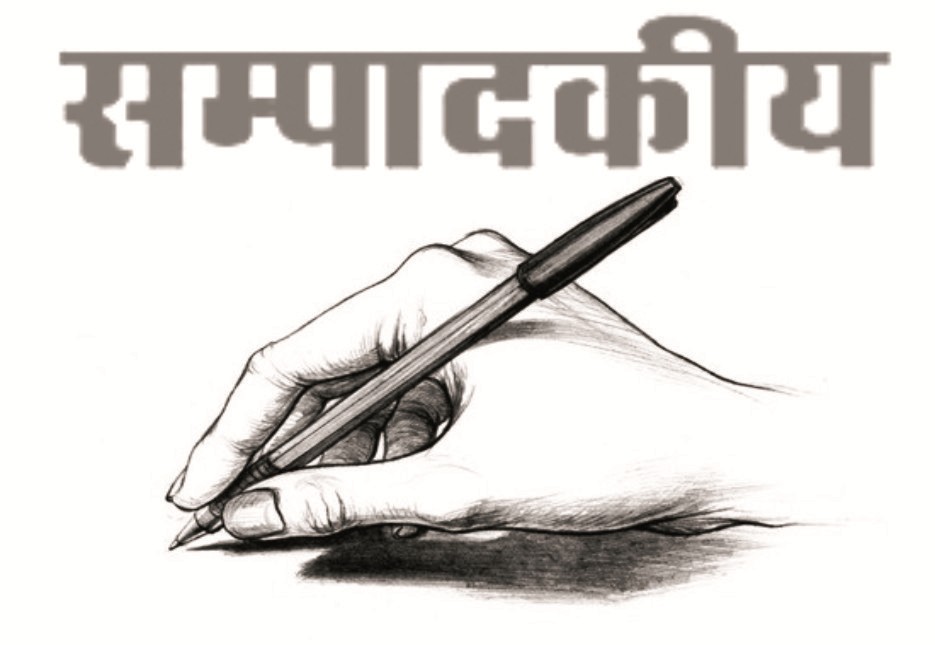
क्या चुनाव आयोग की प्रसांगिता प्रश्नित होती जा रही है? यह सवाल पांच राज्यों के लिये हो रहे विधानसभा चुनाव के परिदृश्य में एक बड़ा सवाल बनकर सामने आया है। क्योंकि इस चुनाव की पूर्व संध्या पर जिस तरह से प्रधानमंत्री का साक्षात्कार प्रसारित हुआ और चुनाव आयोग इस पर चुप रहा। इसी तरह योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू भी प्रसारित हुआ। चुनाव आयोग ने इसका भी कोई संज्ञान नहीं लिया। जबकि 2017 के चुनाव में इसी तरह के राहुल गांधी के एक इंटरव्यू पर चैनल के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने और राहुल गांधी को नोटिस जारी करने की कारवाई की गयी थी। 2017 से 2022 तक आते-आते चुनाव आयोग यहां तक पहुंच गया उसके सरोकार बदल गये हैं। ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतें हर चुनाव में आ रही है। इस बार भी उत्तर प्रदेश के हर चरण में यह शिकायतें आ रही हैं। देश के सारे विपक्षी दल ईवीएम की जगह मत पत्रों के माध्यम से चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं। ईवीएम के साथ वीवीपैट की पूरी गणना करने और ईवीएम के साथ मिलान करने की मांग को नहीं माना जा रहा है। क्या इस परिदृश्य में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठते सवालों को नजरअंदाज किया जा सकता है। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर अभी तक आपराधिक मामला दर्ज करके चुनाव रोकने का प्रावधान नहीं हो पाया है। संसद और विधानसभाओं को अपराधियों से मुक्त करवाने तथा एक देश एक चुनाव के दावे सभी सिर्फ जनता का ध्यान बांटने के हथकण्डे होकर रह गये हैं।
इसी चुनाव में एक स्ट्रिंग ऑपरेशन के माध्यम से बसपा और भाजपा के दो बड़े नेताओं के बीच हुई बैठक का एक आडियो/वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कथित रूप से यह कहा गया है कि बसपा की करीब 40 सीटें आयेंगी जिन्हें तीन सौ करोड़ लेकर भाजपा को सौंप दिया जायेगा। इस आडियो/ वीडियो का भाजपा और बसपा द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। इसी तरह पंजाब के चुनाव को लेकर हुई एक चैनल वार्ता में भाजपा के प्रतिनिधि ने यहां तक कह दिया कि यदि भाजपा की पच्चीस सीटें भी आ गयी तो सरकार वही बनायेंगे। इस दावे का सीधा अर्थ है कि धन और बाहुबल के सहारे ऐसा किया जायेगा। पंजाब के मतदान की तारीख चौदह फरवरी से बीस कर दी गयी और इसी दौरान बाबा राम रहीम को पांच बार पैरोल मिल गयी। यह संयोग कैसे घटा इसे हर आदमी समझ रहा है। इन सारे मुद्दों पर चुनाव आयोग खामोश रहा और इसी से सवाल उठ रहे हैं क्योंकि चुनाव को बड़े योजनाबद्ध तरीके से धन केंद्रित बनाया जा रहा है। आज भाजपा अपनी घोषित आय के मुताबिक देश का सबसे अमीर राजनीतिक दल बन गया है। इसके लिये जिस तरह के नियमों को बदला गया है उस पर नजर डालने से सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है।
2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय में एफ सी आर ए को लेकर एक याचिका दायर हुई जिसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों को दोषी पाते हुए इनके खिलाफ छः माह के भीतर कारवाई करने के निर्देश चुनाव आयोग को दिये गये थे। लेकिन चुनाव आयोग के कुछ करने से पहले ही 2016 में सरकार ने विदेशी कंपनी की परिभाषा बदल दी और इसे 2010 से लागू कर दिया। इसके बाद फाइनेंस एक्ट की धारा 154 और कंपनी एक्ट की धारा 182 बदल दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस बदलाव को अस्वीकार करते हुए फिर भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ आयोग को कारवाई के निर्देश दिये। लेकिन 2018 में सरकार ने एफ सी आर ए में 1976 से ही बदलाव करके विदेशी कंपनियों से लिये गये चन्दे को वैध करार दे दिया और चन्दा देने की सीमा बीस हजार से घटाकर दो हजार कर दी। अब इलेक्ट्रोरल बॉन्ड लाकर सारा परिदृश्य ही बदल दिया गया है। इस इलेक्ट्रोरल बॉन्ड के जरिये कोई भी किसी भी पार्टी को कितना भी चन्दा दे सकता है क्योंकि बॉन्ड एक वीयर्र चेक की तरह है जिस पर न खरीदने वाले का नाम होगा और न ही इसको भुनाने वाले दल का नाम होगा। पन्द्रह दिन के भीतर इसे कैश करना होता है। एक वर्ष में जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर में दस-दस दिनों के लिए बॉन्ड खरीद खोली जाती है। एस बी आई की 29 शाखाओं से यह खरीदे जा सकते हैं जो राज्यों के राजधानी नगरों में स्थित हैं। एक लाख से लेकर एक करोड़ तक का चन्दा इसके माध्यम से दिया जा सकता है। इन बॉन्डस को लेकर चुनाव आयोग लगातार मूकदर्शक की भूमिका में रहा है जबकि इन बॉन्डस के माध्यम से ब्लैक मनी का आदान-प्रदान हो रहा है। क्योंकि कोई भी पंजीकृत दल यह चन्दा लेने का अधिकारी है यदि उसे चुनावों में कम से कम एक प्रतिशत वोट हासिल हुये हैं। अभी पांच राज्यों के चुनावों से पहले जनवरी 2022 के दस दिनों ही चन्दा देने के लिये एस बी आई से 1213 करोड़ के यह बॉन्डस बिके हैं। 2018 से लेकरं अब तक 9207 करोड़ का चन्दा राजनीतिक दलों को इनके माध्यम ये मिला है। क्या इस तरह के चन्दे से चुनाव केवल पैसे के गिर्द ही केंद्रित होकर नहीं रह जायेंगे? क्या यह एक प्रभावी लोकतंत्र बनाने में सहायक हो पायेंगे? क्या चुनाव आयोग की स्वायत्तता का यही अर्थ है कि वह इस सब को देखकर अपनी आंखें और मुंह बन्द रखे?
बैंक फ्राड के माध्यम से लूट कब तक
- Details
- Created on Tuesday, 15 February 2022 19:11
- Written by Shail Samachar





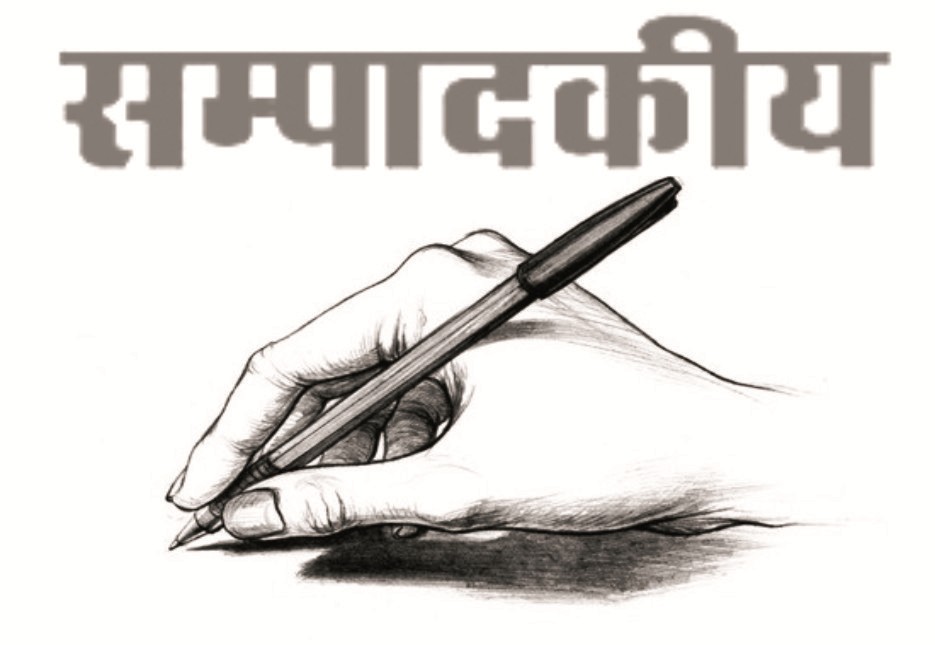
आज यदि 2014 की तुलना में महंगाई और बेरोजगारी का आकलन किया जाये तो इसमें 100 प्रतिशत से भी ज्यादा की बढ़ौतरी हुई है और इसी अनुपात में देश की 80 प्रतिशत से अधिक की जनता के आय के साधन नहीं बढ़े हैं। बल्कि इस दौरान बैंकों में जमा आम आदमी के जमा पर ब्याज दर कम हुई है। यही नहीं जीरो बैलेंस के नाम पर खोले गये बैंक खातों में न्यूनतम बैलेंस 1000 और डाकघरों में 500 रखने की शर्त लागू है। इस न्यूनतम पर खाता धारक को कुछ नहीं मिल रहा है। जबकि बैंकों को इससे कमाई हो रही है। इस संदर्भ में यह कहना ज्यादा सही होगा कि सरकार इन लुटेरों की लूट की भरपाई आम आदमी की जेब पर अपरोक्ष में डाका डाल कर रही है। इस लूट और डाके पर हिंदू-मुस्लिम मंदिर-मस्जिद हिजाब और धारा 370 तथा तीन तलाक के मुद्दे खड़े करके बहस को लंबित किया जा रहा है। लेकिन यह तय है कि देर सवेर महंगाई और बेरोजगारी जब बर्दाश्त से बाहर हो जायेंगी तब जो रोष का सैलाब आयेगा वह सब कुछ अपने साथ बहाकर ले जायेगा। क्योंकि जब बैंकों का एनपीए सरकार की राजस्व आय से बढ़ जाता है तो उस बैंकिंग व्यवस्था को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। यह सरकार इस लूट के लाभार्थियों पर हाथ डालने की स्थिति में नहीं है। सरकार ने क्रिप्टो को अभी तक लीगल करार नहीं दिया है लेकिन इससे हुई कमाई पर टैक्स लेने की घोषणा बजट में कर रखी है। यह अपने में स्वतः विरोध है और इसी तरह के विरोधों पर यह सरकार टिकी हुई है। अब नीति आयोग सीधे नीति बनाकर सरकार को दे रहा है। नीति निर्धारण में संसद की भूमिका नहीं के बराबर रह गई है।
इस परिदृश्य में यह सवाल और भी अहम हो गया है कि प्रधानमंत्री इस सब पर चुप क्यों है? क्या सत्तारूढ़ भाजपा को इस लूट में हिस्सा मिल रहा है? यह हिस्से की चर्चा इसलिये उठ रही है क्योंकि इस समय भाजपा की घोषित संपत्ति वर्ष 2019-20 के लिए 4847.78 करोड़ दिखाई गई है। यह संपत्ति कार्यकर्ताओं के चंदे से संभव नहीं है। तय है कि इसके लिये बड़े घरानों से चुनावी बॉंडस के माध्यम से बड़ा चंदा आया है और यह बॉंडस गोपनीयता के दायरे में आते हैं इसलिए सार्वजनिक नहीं हो रहे। इसी कारण से लूट पर चुप्पी साधनी पड़ रही है। लेकिन इन चुनावों में जिस तरह से किसान समुदाय ने भाजपा का विरोध किया है उसमें आने वाले दिनों में जब महंगाई और बेरोजगारी से पीड़ित आम आदमी भी शामिल हो जायेेगा तो एकदम स्थितियां बदल जायेंगी यह तय है।
गरीब और ग्रामीण के हितों की अनदेखी का बजट
- Details
- Created on Monday, 07 February 2022 15:22
- Written by Shail Samachar





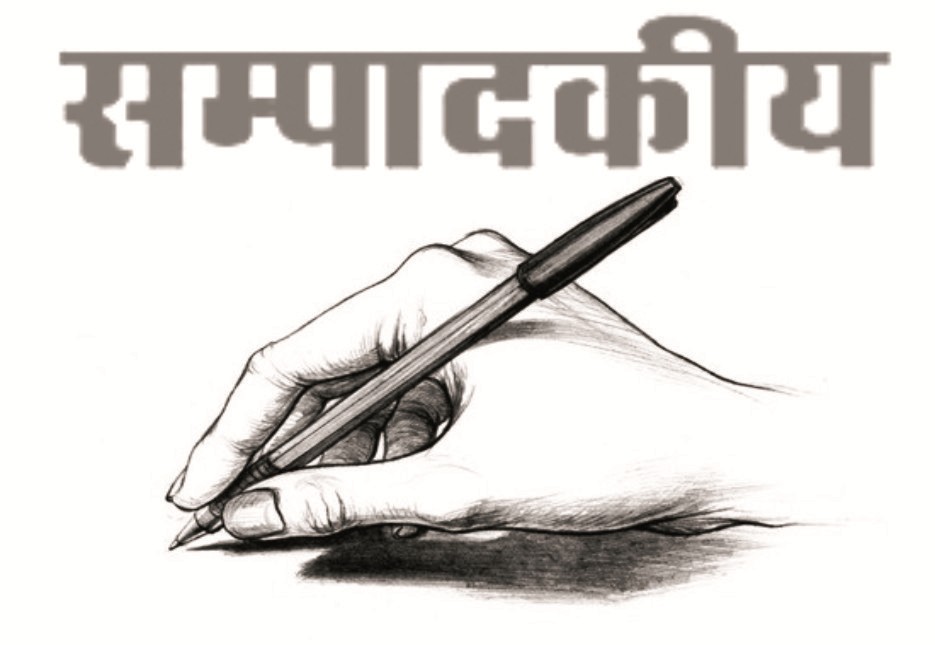
वित्त मंत्री ने 39.45 करोड़ का कुल बजट लोकसभा में पेश किया है। पिछले वर्ष के मुकाबले इसमें 4.6 प्रतिशत की वृद्धिहै। इस कुल खर्च के मुकाबले सरकार की सारे साधनों से आय 22.84 लाख करोड़ हैं और शेष 16.61 लाख करोड़ कर्ज लेकर जुटाया जायेगा। इस कर्ज के साथ सरकार का कुल कर्ज जीडीपी का 60% हो जायेगा। इस कर्ज पर दिया जाने वाला ब्याज सरकार की राजस्व आय का 43% हो जायेगा। कर्ज की स्थिति हर वर्ष बढ़ती जा रही है और बढ़ते कर्ज के कारण बेरोजगारी तथा महंगाई दोनों बढ़ते हैं यह एक स्थापित सत्य है। इसे अच्छी अर्थव्यवस्था माना जाये या नहीं यह पाठक स्वंय विचार कर सकते हैं। क्योंकि कर्ज का आधार बनने वाले जीडीपी में उत्पादन और सेवायें भी शामिल रहती है जो देश में कार्यरत विदेशी कंपनियों द्वारा प्रदान की जाती है। जबकि इसकी आय देश की आय नहीं होती है। इस परिपेक्ष में सरकार के बजटीय आवंटन पर नजर डालने से सरकार की प्राथमिकताओं का खुलासा सामने आ जाता है । सरकार बड़े अरसे से किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा और दावा करती आ रही है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों और गरीबों के लिए जो आवंटन किए गए हैं उनसे नहीं लगता कि सरकार सही में इसके प्रति गंभीर है। क्योंकि ग्रामीण विकास के लिए पिछले वर्ष के मुकाबले बजट में दस प्रतिश्त की कमी की गयी है। इस कमी से क्या सरकार यह नहीं मानकर चल रही है कि अब गांव के विकास के लिए सरकार को और निवेश करने की जरूरत नहीं है। या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में भी सरकारी संपत्तियों का मौद्रीकरण के नाम पर प्राइवेट सैक्टर को सौंपने की तैयारी है।
ग्रामीण विकास में मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार मिलने लगा था। जब प्रवासी मजदूरों का लॉकडाउन में गांव के लिये पलायन हुआ था तब उन्हें मनरेगा से ही सहारा दिया गया था। इस बार मनरेगा के बजट में 25.5% की कटौती कर दी गयी है। क्या इससे गांव में रोजगार प्रभावित नहीं होगा। इसी तरह पीडीएस में भी 28.5 प्रतिशत की कटौती की गयी है क्या इस कटौती से गरीबों को मिलने वाले सस्ते राशन की कीमतों में असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह रासायनिक खाद्य में 24% पेट्रोल में 10% फसल बीमा में 3% और जल जीवन में 1.3% की कटौती की गयी है। इस तरह इन सारी कटौतियों को देखा जाये तो यह सीधे गांव के आदमी को प्रभावित करेंगे। इन कटौतियों से क्या यह माना जा सकता है कि इससे गरीब और किसान का किसी तरह से भी भला हो सकता है। क्योंकि इसी के साथ किसानी से जुड़ी चीजों को प्राइवेट सैक्टर को दिया जा रहा है। जिसमें खाद्य और बिजली का उत्पादन तथा वितरण आदि शामिल है। यह सारे क्षेत्र वह हैं जिनमें अभी लंबे समय तक सरकार के सहयोग की आवश्यकता है लेकिन सरकार जब इसमें अपना हाथ पीछे खींच रही हैं तो यह कैसे मान लिया जाये कि सरकार इन वर्गों की हितैशी है। लॉकडाउन में इस लेबर कानूनों से संशोधन करके उनका हड़ताल का अधिकार छीन लिया गया है।
बजट में आये इन आबंटनों से स्पष्ट हो जाता है कि यह सारा कुछ एक नीयत और नीति के तहत किया जा रहा है जिसे किसी भी तरह से गरीब और किसान के हित में नहीं कहा जा सकता ।
विश्वास के संकट में भाजपा और मोदी
- Details
- Created on Monday, 31 January 2022 12:37
- Written by Shail Samachar





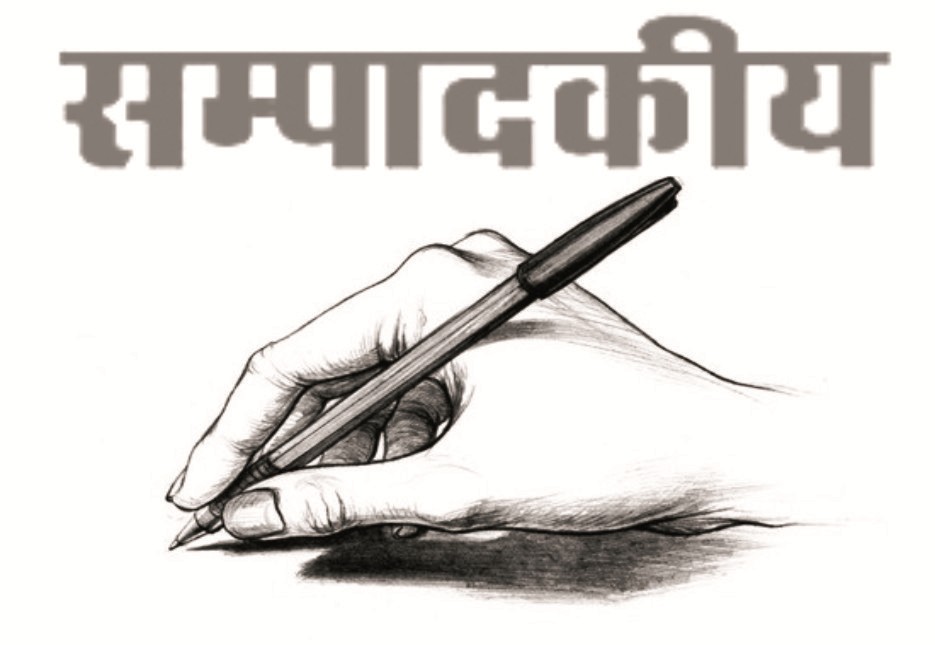
यह सही है कि चुनावों में इस तरह की मुफ्तखोरी के वादे और वह भी सरकारी कोष के माध्यम से सीधे रिश्वतखोरी करार देकर इस पर आपराधिक मामले दायर होने चाहिए और ऐसे दलों की मान्यता रद्द कर दी जानी चाहिय? लेकिन क्या यह मुद्दे उठाने का समय अब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद ही है? क्या ऐसे वादों के दोषी यही दो दल हैं? जब 2014 में हर आदमी के खाते में पन्द्रह-पन्द्रह लाख आने का वायदा किया गया था तब क्या वह जायज था? आज हर सरकार हर वर्ष कर मुक्त बजट देने की घोषणा के पहले या बाद में जनता पर करों का बोझ डालती है क्या यह जायज है? चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी के खर्च की सीमा तो तय कर रखी है लेकिन उसे चुनाव लड़वा रहे दल की को खर्च की सीमाओं से मुक्त रखा है क्यों? चुनाव आयोग हर चुनाव से पहले आचार संहिता की घोषणा करता है। लेकिन इस आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर आपराधिक मामला दर्ज करने का प्रावधान नहीं है। केवल चुनाव याचिका ही दायर करने का प्रावधान है। ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर एक बड़ी राष्ट्रीयव्यापी बहस की आवश्यकता है और तब चुनाव अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिये। लेकिन आज इस ओर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से वायदा किया था कि वह संसद और विधानसभाओं को अपराधियों से मुक्त करवायेंगे। देश में ‘एक देश एक चुनाव’ की व्यवस्था बनाने का भी भरोसा दिया था। लेकिन इन वायदों पर कुछ नहीं हुआ। यदि नीयत होती तो संसद में इतना प्रचंड बहुमत मिलने पर चुनाव अधिनियम में आदर्श संशोधन किये जा सकते थे। परंतु एक ही काम किया कि चुनावी बॉडस के लिये सारा तंत्र सत्तारूढ़ दल के गिर्द घुमाकर रख दिया।
इस परिपेक्ष में आज जो प्रयास किये जा रहे हैं उनकी ईमानदारी पर संदेह होना स्वाभाविक हो गया है। ऐसे में सर्वाेच्च न्यायालय से यही आग्रह रहेगा कि इन चुनावों के परिणाम आने के बाद राजनीतिक दलों की इस मुफ्ती रणनीति पर कड़े प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया जाये जो हर छोटे-बड़े दल पर एक सम्मान लागू हो। चुनाव लड़ने वाले हर व्यक्ति और राजनीतिक दल के लिये यह अनिवार्य किया जाना चाहिये कि वह चुनाव में आने पर नामांकन के साथ ही राज्य या केंद्र जिसके लिये भी चुनाव हों वह आर्थिक स्थिति पर अपना पक्ष स्पष्ट करें और यह घोषणा करे की अपने वायदों को पूरा करने के लिये सरकारी कोष पर न कर्ज का बोझ डालेगा और न ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जनता पर करों का भार डालेगा। न ही सरकारी संपत्तियों का मौद्रीकरण के नाम पर प्राइवेट सैक्टर के हवाले करेगा। जैसा कि इस सरकार ने कर रखा है। आज स्थिति या हो गयी है कि यह सरकार किसानों से राय लिये बिना तीन कृषि कानून लायी। इन कानूनों के विरोध में आंदोलन हुआ। तेरहा माह चले इस आंदोलन में सात सौ किसानों की मौत हो गयी उसके बाद कानूनों को वापस ले लिया गया। स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसपी पर कमेटी बनायेंगे। किसानों के खिलाफ बनाये गये आपराधिक मामले वापिस लिये जायेंगे। लेकिन आज चुनावों के दौरान यह स्पष्ट हो गया है कि इन वायदों पर अमल नहीं हुआ है। इस वादाखिलाफी की आंच चुनाव में साफ असर दिखा रही है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि जब प्रधानमंत्री स्वयं घोषणा करके उस पर चुनाव के वक्त भी अमल न करें तो उसे कैसे लिया जाये। जब प्रधानमंत्री के वायदों पर ही विश्वास न बन पाये तो सरकार और पार्टी पर कोई कैसे विश्वास कर पायेगा? आज प्रधानमंत्री और उनकी सरकार तथा पार्टी सभी एक साथ विश्वास के संकट में हैं और यह सबसे ज्यादा घातक है।