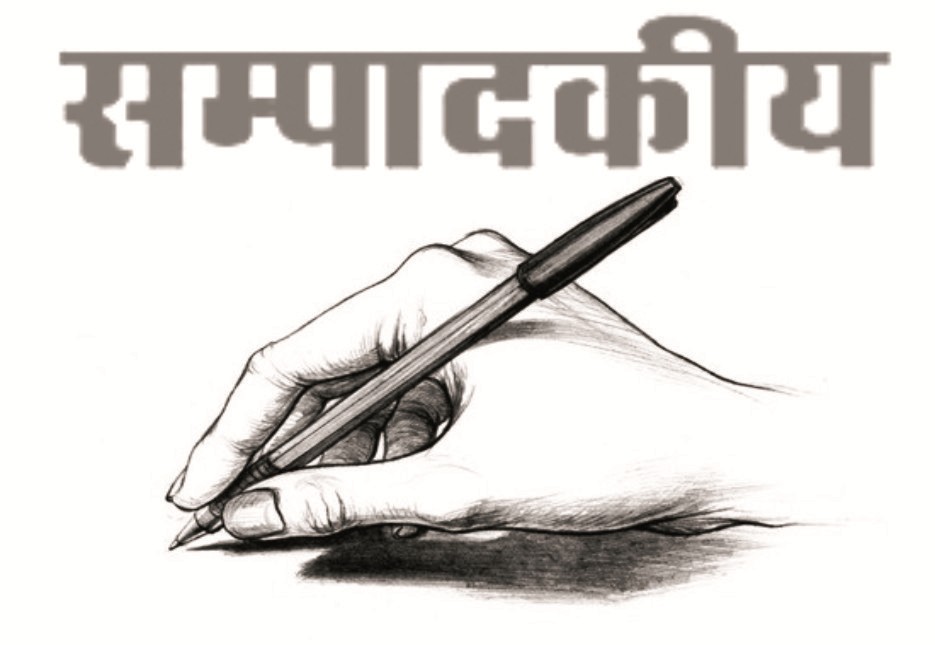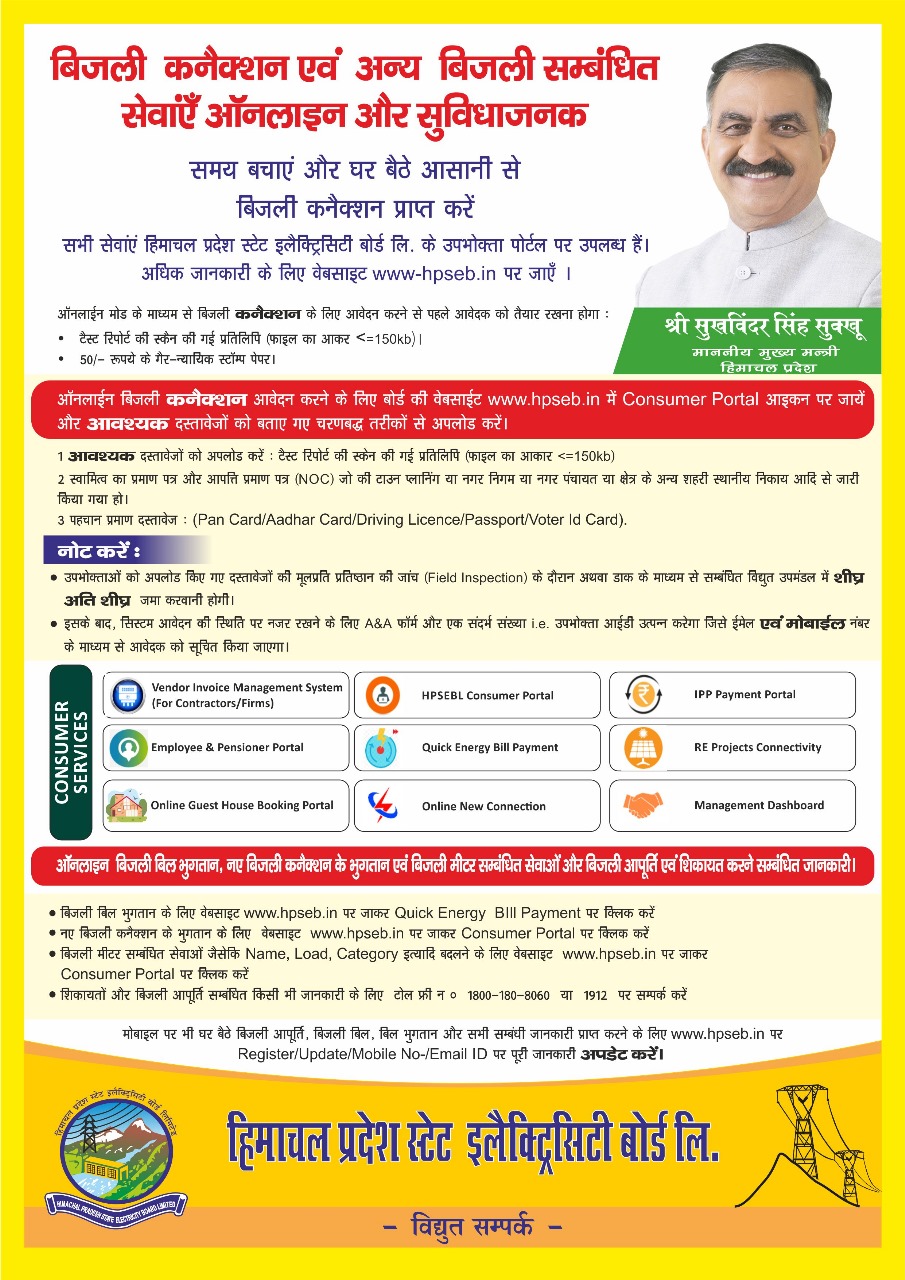ShareThis for Joomla!
क्यों बना है नफरती ब्यानों का वातावरण
- Details
- Created on Tuesday, 27 September 2022 04:59
- Written by Shail Samachar
 नफरती ब्यानों से हुई वस्तुस्थिति पर उभरी चिन्ताओं पर चिन्तन को लेकर सर्वाेच्च न्यायालय के जस्टिस के.एम.जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश राय की खण्डपीठ के पास सुदर्शन टीवी द्वारा दिखाये यूपीएससी जिहाद शो और धर्म संसदों में दिये गये ब्यानों तथा कोविड महामारी के दौरान एक समुदाय विशेष को चिन्हित व इंगित करते हुए सोशल मीडिया के मंचों पर आयी टिप्पणियों पर आयी याचिकाएं निपटारे के लिये लगी हैं। शीर्ष न्यायालय ने इस पर गंभीर चिन्ता व्यक्त करते हुए यह प्रश्न उठाया है कि आखिर देश जा कहां जा रहा है? अदालत ने इस पर सरकार की मुकदर्शिता पर भी चिन्ता व्यक्त करते हुये इस संद्धर्भ में एक सख्त नियामक तंत्र गठित किये जाने पर आवश्यकता पर बल दिया है। सरकार से इस पर अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा है। सर्वाेच्च न्यायालय में उठे सवालों में ही कमीशन की सिफारिश और चुनाव आयोग के सुझाव भी चर्चा में आये हैं। यह भी सामने आया है कि कानून में नफरती ब्यान और अफवाह तक परिभाषित नहीं है। देश के 29 राज्यों में से केवल 14 ने ही इस पर अपने विचार रखे हैं यह सामने आने के बाद सर्वाेच्च न्यायालय ने राज्यों को अपनी राय शीर्ष अदालत में रखने के निर्देश दिये हैं। शीर्ष अदालत में यह सब घटने के बाद कुछ टीवी चैनलों ने इस मुद्दे पर सार्वजनिक बहस भी आयोजित की है। इस सारे मन्थन से क्या निकल कर सामने आता है यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन आज देश में इस तरह का वातावरण क्यों निर्मित हुआ है? केन्द्र में सत्तारूढ़ पक्ष इस पर क्यों मौन चल रहा है? उसे इससे किस तरह का राजनीतिक लाभ मिल रहा है? इस मन्थन से इन सवालों का कोई सीधा संद्धर्भ नहीं उठाया जा रहा है। जबकि मेरा मानना है कि यह सवाल इस बहस का केन्द्र बिन्दु होने चाहिये। अदालत ने भी सरकार की खामोशी पर सवाल उठाते हुए एक सख्त नियामक तन्त्र के गठन की बात की है। आज केन्द्र में वह राजनीतिक दल सत्तारूढ़ है जिसका वैचारिक नियन्त्रण आर.एस.एस. के पास है। 1947 में देश की आजादी के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने वैचारिक धरातल को विस्तार देने के लिये 1948 और 1949 में ही युवा संगठन के नाम पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का गठन करने के साथ ही हिन्दुस्तान समाचार एजेन्सी का गठन कर लिया। यह वह क्रियात्मक कदम थे जिन से आने वाले वक्त में मीडिया यूथ की भूमिका का आकलन उसी समय कर लिया गया। उसके बाद आगे चलकर इसकी अनुषंागिक इकाइयों संस्कार भारती और इतिहास लेखन प्रकोष्ठ आदि का गठन इस दिशा के दूसरे मील के पत्थर सिद्ध हुए हैं। इसी सबका परिणाम संघ के सनातकों के रूप में सामने आया। मजे की बात तो यह है कि यह स्नातक लाखों की संख्या में तृतीय वर्ष पास करके आ चुके हैं। अधिकांश राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों में शामिल हो चुके हैं लेकिन इस पाठयक्रम को लेकर चर्चा नहीं के बराबर रही है। आज के नये राजनीतिक कार्यकर्ताओं से चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हो यदि यह पूछा जाये कि संघ का आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक चिन्तन क्या है तो वह शायद कुछ भी न बता पायें। उनकी नजर में यह एक सांस्कृतिक संगठन है जिसकी सांस्कृतिक विरासत मनुस्मृति से आगे नहीं बढ़ती। इसी संस्कृति का परिणाम है कि आज समाज का एक बड़ा वर्ग न्यायपालिका से लेकर राजनेताओं तक हिन्दू राष्ट्र के एजेंडे में शामिल हो चुका है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 1998 के राष्ट्रीय अधिवेशन में त्रीस्तरीय संसद के गठन का प्रस्ताव पारित होने के बाद आज हालात इन ब्यानों तक पहुंच गये हैं। स्कूलों में मनुस्मृति को पाठयक्रम का हिस्सा बनाने की बात हो रही है। क्योंकि जब गुजरात दीन्नानाथ बत्रा की किताबों को स्कूल पाठयक्रम का हिस्सा बनाया जा रहा था तब इसकी चर्चा तक नहीं उठाई गयी थी। आज संघ की विचारधारा पर जब तक सार्वजनिक बहस के माध्यम से स्वीकार्यता या अस्वीकार्यता तक नहीं पहुंचा जाता है तब तक हिन्दू राष्ट्र के एजेंडे की वकालत के लिए ऐसे नफरती ब्यानों को रोकना आसान नहीं होगा।
नफरती ब्यानों से हुई वस्तुस्थिति पर उभरी चिन्ताओं पर चिन्तन को लेकर सर्वाेच्च न्यायालय के जस्टिस के.एम.जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश राय की खण्डपीठ के पास सुदर्शन टीवी द्वारा दिखाये यूपीएससी जिहाद शो और धर्म संसदों में दिये गये ब्यानों तथा कोविड महामारी के दौरान एक समुदाय विशेष को चिन्हित व इंगित करते हुए सोशल मीडिया के मंचों पर आयी टिप्पणियों पर आयी याचिकाएं निपटारे के लिये लगी हैं। शीर्ष न्यायालय ने इस पर गंभीर चिन्ता व्यक्त करते हुए यह प्रश्न उठाया है कि आखिर देश जा कहां जा रहा है? अदालत ने इस पर सरकार की मुकदर्शिता पर भी चिन्ता व्यक्त करते हुये इस संद्धर्भ में एक सख्त नियामक तंत्र गठित किये जाने पर आवश्यकता पर बल दिया है। सरकार से इस पर अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा है। सर्वाेच्च न्यायालय में उठे सवालों में ही कमीशन की सिफारिश और चुनाव आयोग के सुझाव भी चर्चा में आये हैं। यह भी सामने आया है कि कानून में नफरती ब्यान और अफवाह तक परिभाषित नहीं है। देश के 29 राज्यों में से केवल 14 ने ही इस पर अपने विचार रखे हैं यह सामने आने के बाद सर्वाेच्च न्यायालय ने राज्यों को अपनी राय शीर्ष अदालत में रखने के निर्देश दिये हैं। शीर्ष अदालत में यह सब घटने के बाद कुछ टीवी चैनलों ने इस मुद्दे पर सार्वजनिक बहस भी आयोजित की है। इस सारे मन्थन से क्या निकल कर सामने आता है यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन आज देश में इस तरह का वातावरण क्यों निर्मित हुआ है? केन्द्र में सत्तारूढ़ पक्ष इस पर क्यों मौन चल रहा है? उसे इससे किस तरह का राजनीतिक लाभ मिल रहा है? इस मन्थन से इन सवालों का कोई सीधा संद्धर्भ नहीं उठाया जा रहा है। जबकि मेरा मानना है कि यह सवाल इस बहस का केन्द्र बिन्दु होने चाहिये। अदालत ने भी सरकार की खामोशी पर सवाल उठाते हुए एक सख्त नियामक तन्त्र के गठन की बात की है। आज केन्द्र में वह राजनीतिक दल सत्तारूढ़ है जिसका वैचारिक नियन्त्रण आर.एस.एस. के पास है। 1947 में देश की आजादी के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने वैचारिक धरातल को विस्तार देने के लिये 1948 और 1949 में ही युवा संगठन के नाम पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का गठन करने के साथ ही हिन्दुस्तान समाचार एजेन्सी का गठन कर लिया। यह वह क्रियात्मक कदम थे जिन से आने वाले वक्त में मीडिया यूथ की भूमिका का आकलन उसी समय कर लिया गया। उसके बाद आगे चलकर इसकी अनुषंागिक इकाइयों संस्कार भारती और इतिहास लेखन प्रकोष्ठ आदि का गठन इस दिशा के दूसरे मील के पत्थर सिद्ध हुए हैं। इसी सबका परिणाम संघ के सनातकों के रूप में सामने आया। मजे की बात तो यह है कि यह स्नातक लाखों की संख्या में तृतीय वर्ष पास करके आ चुके हैं। अधिकांश राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों में शामिल हो चुके हैं लेकिन इस पाठयक्रम को लेकर चर्चा नहीं के बराबर रही है। आज के नये राजनीतिक कार्यकर्ताओं से चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हो यदि यह पूछा जाये कि संघ का आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक चिन्तन क्या है तो वह शायद कुछ भी न बता पायें। उनकी नजर में यह एक सांस्कृतिक संगठन है जिसकी सांस्कृतिक विरासत मनुस्मृति से आगे नहीं बढ़ती। इसी संस्कृति का परिणाम है कि आज समाज का एक बड़ा वर्ग न्यायपालिका से लेकर राजनेताओं तक हिन्दू राष्ट्र के एजेंडे में शामिल हो चुका है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 1998 के राष्ट्रीय अधिवेशन में त्रीस्तरीय संसद के गठन का प्रस्ताव पारित होने के बाद आज हालात इन ब्यानों तक पहुंच गये हैं। स्कूलों में मनुस्मृति को पाठयक्रम का हिस्सा बनाने की बात हो रही है। क्योंकि जब गुजरात दीन्नानाथ बत्रा की किताबों को स्कूल पाठयक्रम का हिस्सा बनाया जा रहा था तब इसकी चर्चा तक नहीं उठाई गयी थी। आज संघ की विचारधारा पर जब तक सार्वजनिक बहस के माध्यम से स्वीकार्यता या अस्वीकार्यता तक नहीं पहुंचा जाता है तब तक हिन्दू राष्ट्र के एजेंडे की वकालत के लिए ऐसे नफरती ब्यानों को रोकना आसान नहीं होगा।
यह चुनावी घोषणाएं कहां ले जायेगी
- Details
- Created on Tuesday, 20 September 2022 07:13
- Written by Shail Samachar

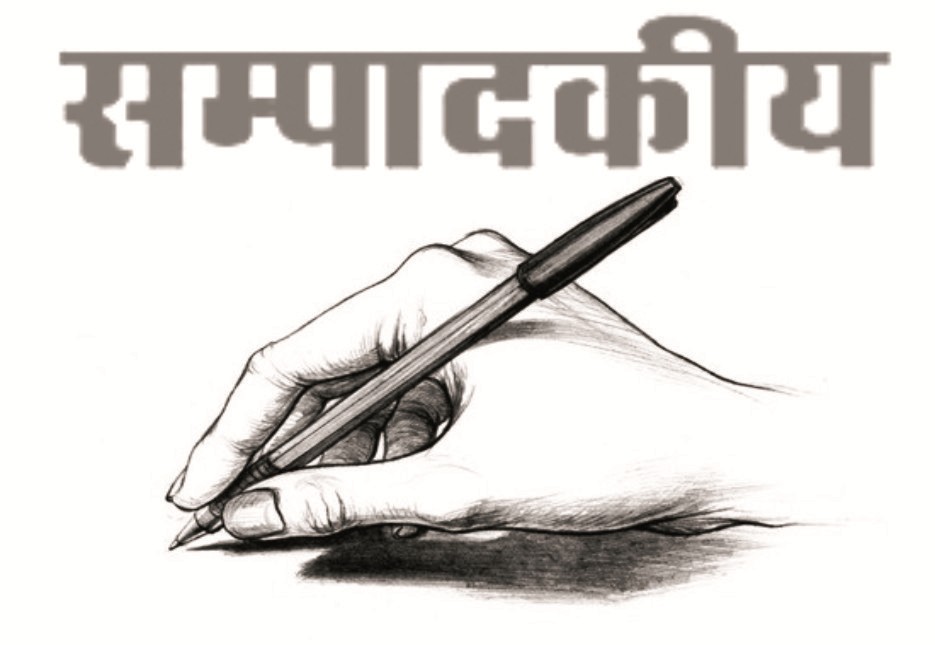
जबकि 31 मार्च 2020 को सदन के पटल पर रखी कैग रिपोर्ट के मुताबिक 2019 तक केन्द्रीय योजनाओं में प्रदेश को एक भी पैसा नहीं मिला है। कैग के मुताबिक ही सरकार 96 योजनाओं में कोई पैसा नहीं खर्च कर पायी है। बच्चों को स्कूल बर्दी तक नहीं दी जा सकी है। कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के एरियर की किस्त तक नहीं दी जा सकी है क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं था। लेकिन 2019 में लोकसभा के चुनाव थे। 2019-20 के बजट दस्तावेज के मुताबिक इस वर्ष सरकार के अनुमानित खर्च और वास्तविक खर्चे में करीब 16,000 करोड़ का अन्तर आया है। कैग रिपोर्ट में यह दर्ज है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक हो जाता है कि जब केन्द्र ने कोई वितिय सहायता नही दी है तो इस बड़े हुये खर्च का प्रबन्ध कर्ज लेकर ही किया गया होगा। कैग रिपोर्ट पर आज तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय और मीडिया तक ने इस रिपोर्ट को शायद पढ़ने समझने का प्रयास नही किया है। इसी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कुल बजट का 90% राजस्व व्यय हो चुका है। विकास कार्यों के लिए केवल 10% ही बचता है। वर्ष 2022-23 के 51,365 करोड़ का 10% ही जब विकास के लिये बचता है तो उसमें आज मुख्यमन्त्री द्वारा की जा रही घोषणाएं कैसे पूरी हो पायेगी? स्वभाविक है कि इसके लिये कर्ज लेने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह जाता है।
आज मुख्यमन्त्री अपनी सरकार की सत्ता में वापसी के लिये हजारों करोड़ों दाव पर लगा रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों की घोषणाएं की जा रही है। अभी अगला चुनावी घोषणा पत्र तैयार हो रहा है। उसमें भी वायदे किये जायेंगे। विपक्ष भी इसी तर्ज पर घोषणा पत्रों से पहले ही गारटियों की प्रतिस्पर्धा में आ गया है। केन्द्र द्वारा प्रदेश को जो कुछ भी देना घोषित किया गया है वह अब तक सैद्धांतिक स्वीकृतियों से आगे नहीं बढ़ पाया है। प्रदेश के घोषित 69 राष्ट्रीय राजमार्ग इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर सरकार श्वेत पत्र जारी करने के लिये तैयार नहीं है और न ही विपक्ष इसकी गंभीरता से मांग कर रहा है। जयराम सरकार को विरासत में 46,385 करोड़ का कर्ज मिला था लेकिन आज यह कर्जभार कहां पहुंच गया है इस पर कुछ नहीं कहा जा रहा है। 1,76,000 करोड़ की जी.डी.पी. वालेे प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के कर्ज को मिलाकर यह आंकड़ा एक लाख करोड़ तक पहुंचना क्या चिन्ता का विषय नहीं होना चाहिये यह पाठकों के आकलन पर छोड़ता हूं।
वक्त की जरूरत है भारत जोड़ो यात्रा
- Details
- Created on Wednesday, 14 September 2022 07:18
- Written by Shail Samachar




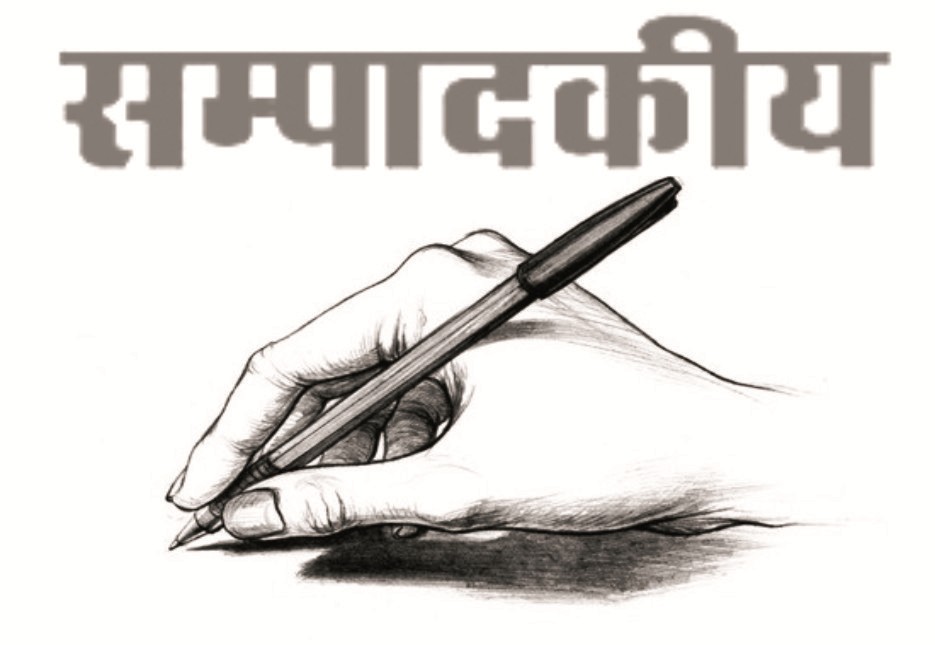
इस परिदृश्य में यह तलाशना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज यह यात्रा वक्त की जरूरत क्यों बन गयी। इसके लिये अगर अपने आस पास नजर दौड़ायें तो सामने आता है कि सत्तारूढ़ भाजपा ने विपक्ष की सरकारों को गिराने के लिये केन्द्रीय जांच एजेन्सियों का इस्तेमाल किस हद तक बढ़ा दिया है। इन एजेन्सियों के बढ़ते दखल ने इनकी विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिये हैं। पिछले काफी समय से संघ प्रमुख डॉ. मनमोहन भागवत के नाम से भारत के नये संविधान के कुछ अंश वायरल होकर बाहर आ चुके हैं। लेकिन इस पर न तो केन्द्र सरकार और न ही संघ परिवार की ओर से कोई खण्डन आया है। बल्कि मेघालय उच्च न्यायालय के जस्टिस सेन के दिसंबर 2018 में आये हिन्दू राष्ट्र के फैसले और अब डॉ. स्वामी की संविधान से धर्म निरपेक्षता तथा समाजवाद शब्दों को हटाने के आग्रह की सर्वाेच्च न्यायालय में आयी याचिका ने इन आशंकाओं को और बढ़ा दिया है। क्या आज के भारतीय समाज में यह सब स्वीकार्य हो सकता है।
2014 के लोकसभा चुनावों से पहले अन्ना आन्दोलन के माध्यम से भ्रष्टाचार के जिन मुद्दों को उछाला गया था क्या उनमें से एक भी अन्तिम परिणाम तक पहुंचा है? क्या आज भाजपा शासित राज्यों में सभी जगह लोकायुक्त नियुक्त है? क्या सभी राज्यों में मानवाधिकार आयोग सुचारू रूप से कार्यरत हैं? क्या इस दौरान हुये दोनों लोकसभा चुनावों में हर बार चुनावी मुद्दे बदले नहीं गये हैं? इस दौरान नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक जितने भी आर्थिक फैसले लिये गये हैं क्या उनसे देश की आर्थिकी में कोई सुधार हो पाया है? क्या सार्वजनिक संस्थानों को प्राइवेट सैक्टर के हवाले करना स्वस्थ्य आर्थिकी का लक्षण माना जा सकता है? आज जब शिक्षा और स्वास्थ्य को पीपीपी मोड के माध्यम से प्राइवेट सैक्टर को देने की घोषणा की जा चुकी है तब क्या यह उम्मीद की जा सकती है कि यह आवश्यक सेवाएं आम आदमी को सुगमता से उपलब्ध हो पायेंगी? कल तक यह कहा जा रहा था कि चीन हमारी सीमा में घुसा ही नहीं है परन्तु अब यह कहा जा रहा है कि चीन वापिस जाने को तैयार हो गया है। कुल मिलाकर राष्ट्रीय महत्व के हर मुद्दे पर लगातार गलत ब्यानी हो रही है और उसे हिन्दू-मुस्लिम तथा मन्दिर-मस्जिद के नाम पर नया रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। आज इन सवालों को आम आदमी के सामने ले जाने की आवश्यकता है और इस काम के लिये किसी बड़े नेता को ही भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से इस काम को अन्जाम देना होगा। राहुल गांधी की यात्रा से सता पक्ष में जिस तरह की प्रतिक्रियाएं उभर रही हैं उससे स्पष्ट हो जाता है कि यह यात्रा सही वक्त पर सही दिशा में आयोजित की गयी है।
क्या धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद संविधान से हटा देना चाहिये?
- Details
- Created on Monday, 05 September 2022 13:37
- Written by Shail Samachar




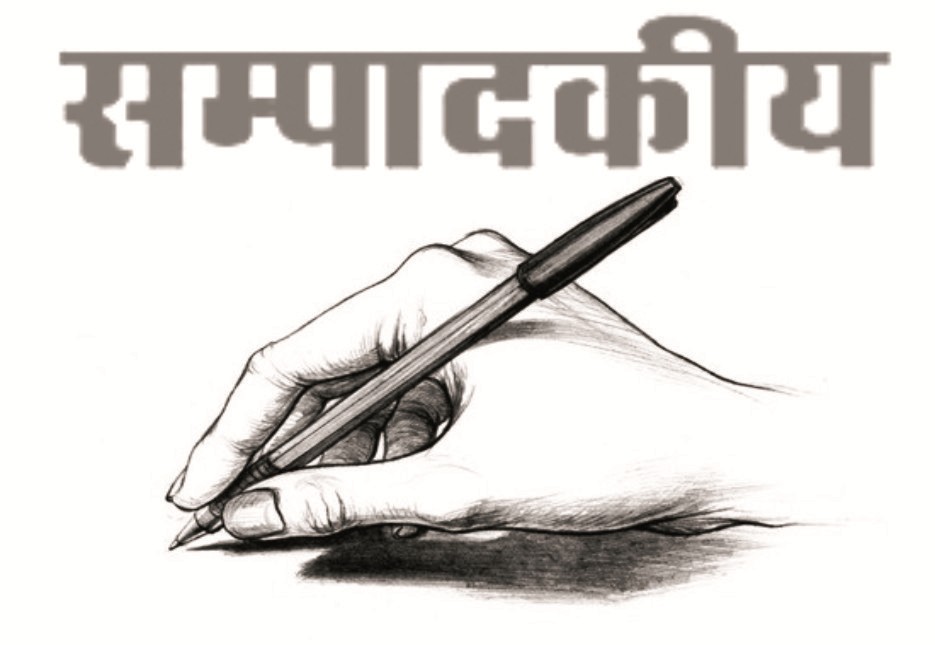
कर्ज लेकर मुफ्त कब तक बांटा जा सकता है
- Details
- Created on Monday, 29 August 2022 02:28
- Written by Shail Samachar