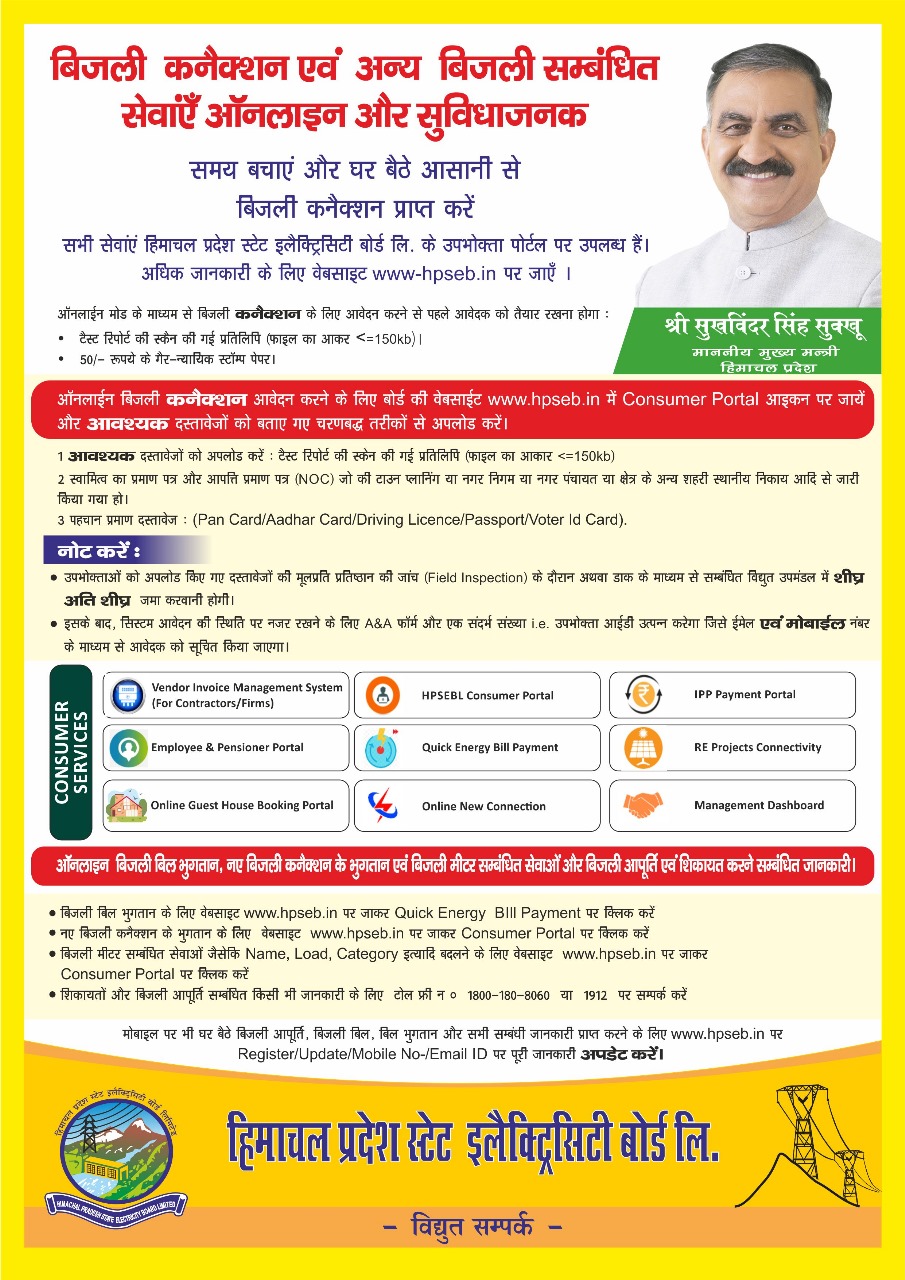ShareThis for Joomla!
कोविड को लेकर "Covid Vaccination Voluntary, Hasn't Mandated Vaccination" केंद्र सरकार का सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र
- Details
- Created on Monday, 06 December 2021 17:18
- Written by Shail Samachar
क्या इस शपथ पत्र के बाद भी कोई अधिकारी टीकाकरण के आदेश जारी कर पायेगा
क्या आरोग्य सेतु एप पर भी सरकार का ऐसा ही स्टैंड नहीं रहा है

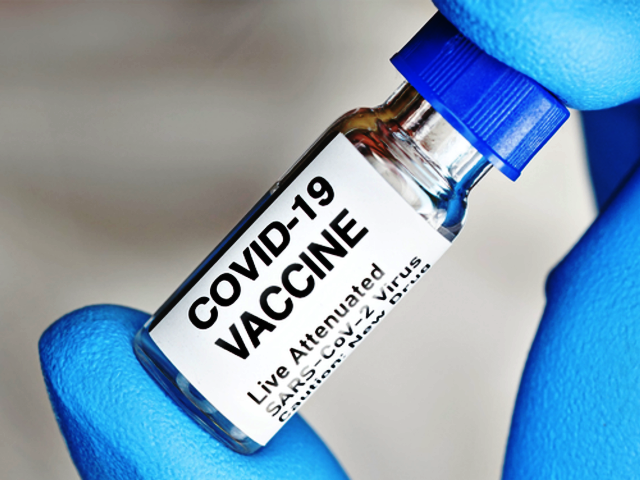
यदि पिछले कुछ वर्षों पर नजर डाली जाए तो यह सामने आता है कि हर 10-12 वर्ष के अंतराल में कोई न कोई बीमारी आती रही है। कोविड-19 से पहले स्वाइन फ्लू था। और स्वाइन फ्लू तथा कोविड के लक्षणों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों एक जैसे ही गंभीर कहे गये हैं। देश में हर जन्म और मरण का पंजीकरण होता है यह नियम है। मरण के आंकड़े संसद में गृह मंत्रालय के तहत रजिस्ट्रार जनरल द्वारा रखे जाते हैं। 2018 तक के आंकड़े संसद में रखे जा चुके हैं और इनके अनुसार देश में 2018 में 69 लाख लोगों की मौत हुई है। हिमाचल का आंकड़ा ही 48000 रहा है। इसी आंकड़े के में स्वाइन फ्लू से हुई मौतें भी शामिल हैं। लेकिन इन मौतों के बावजूद भी कोई लॉकडाउन घोषित नही किया गया था और न ही वैक्सीनेशन के लिए आज की तरह कोई स्पेशल ड्राइव शुरू किया गया था। जबकि फरवरी 2020 में भी आईजीएमसी शिमला के अतिरिक्त मंडी और धर्मशाला में स्वाइन फ्लू के मरीज दाखिल थे। उस दौरान भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक पत्रकार वार्ता में स्पेशल आईसीयू बनाने के निर्देश दिये थे।
लेकिन कोविड-19 के मामले में देश में 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन घोषित कर दिया गया जो कई चरणों में चला। इस लॉकडाउन के कारण अस्पतालों में ओपीडी और इन डोर दोनों सेवाएं बंद हो गई। उस समय अकेले आईजीएमसी का ओपीडी का 2018 का आंकड़ा 8 लाख रहा है। यदि उस समय अस्पताल में दाखिल मरीजों का 1ः भी गंभीर रहा होगा तो उसका इलाज बंद होने पर उसकी क्या स्थिति रही होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कोविड कि वैक्सीन तो 16 जनवरी 2021 से शुरू हुई लेकिन इसका निर्माण लॉकडाउन से पहले ही हो चुका था यह तथ्य सामने आ चुका है। अप्रैल 2020 को तो एक डॉ. कुनाल शाह ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके इसके संभावित इलाज पर कुछ आशंकाएं उठाई थी। जिन्हें जस्टिस रमना की पीठ ने आईसीएमआर को भेज दिया था। इसी दौरान अजीम प्रेम जी के सहयोग से उनके एक नागपुर स्थित एनजीओ साथी की एक स्टडी भी सामने आई जिसमें खुलासा किया गया है कि फॉर्मा कंपनियां अपनी दवाएं प्रमोट करने के लिए किस तरह के हथकंडे अपनाती हैं। फार्मा कंपनियों की इसी तरह की भूमिका का पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने भी अपनी आत्मकथा में उल्लेख किया है। आज भी सरकार के पास ऐसी कोई स्टडी नहीं है की लॉकडाउन से पूर्व जो लोग ओपीडी और इन डोर होकर इलाज करवा रहे थे उनमें से इलाज बंद होने पर कितने कोविड के संक्रमण का शिकार हुये और मर गये। आज यह सारे सवाल इसलिये प्रसांगिक हो जाते हैं की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र देकर यह कहां है की वैक्सीनेशन अनिवार्य नहीं वर्ण एच्छीक है। क्या इस शपथ पत्र के बाद कोई भी अधिकारी वैक्सीनेशन को लेकर कोई लिखित आदेश करेगा। आज जो स्टैंड वैक्सीनेशन को लेकर लिया गया है पूर्व में ऐसा ही स्टैंड आरोग्य सेतु एप को लेकर भी रहा है।
अब जब केंद्र सरकार ने शपथ पत्र देकर यह कहा कि वैक्सीनेशन ऐच्छिक है और इसे वैधानिक अनिवार्यता नहीं बनाया गया है तब यह सवाल उठना भी स्वाभाविक है। इसको लेकर जो अन्य मास्क आदि को लेकर जो निर्देश जारी किये गये हैं और उनकी अनुपालना न किये जाने पर जो जुर्माना आदि लगाया जा रहा है उसका वैधानिक आधार क्या है। क्योंकि किसी भी बीमारी का सबसे बड़ा पक्ष उसकी दवाई होता है। यह वैक्सीनेशन इस बीमारी में दी जाने वाली कोई दवाई नहीं है इससे केवल इसके संक्रमण से कुछ समय के लिए बचा जा सकता है। यह भी नहीं है कि वैक्सीनेशन लेने के बाद आदमी कोविड का संक्रमित नहीं हो सकता। इसलिए जो लोग इस बीमारी को महामारी की संज्ञा देने का विरोध करते हुये इसे सामान्य बीमारियों की तरह ही लेने की राय दे रहे थे वह शायद सही थे। 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगाकर जिस तरह की बंदीशें लगा दी गई थी और उनसे जिस तरह का नकारात्मक प्रभाव देश की आर्थिकी और अन्य क्षेत्रों पर पड़ा है उस सब पर सरकार के इस शपथ पत्र के बाद देर सवेर जो सवाल और चर्चाएं उठाएंगे उनका अंतिम परिणाम कहीं आपातकाल में लाये गये नसबंदी अभियान जैसा ही न हो इसकी संभावनाएं बनती जा रही है।